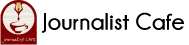हेमंत शर्मा की इतवारी कथा: ज्यों कीं त्यों धर दीनी चदरिया
अज़ीज़ भाई मेरे बेहद अज़ीज़ थे।वे बनारसी साड़ियॉं बुनते थे।जरी और सिल्क की अलग अलग डिजाइन वाली जैसी खूबसूरत साड़ियाँ वे बुनते थे, वैसा ही वैविध्यपूर्ण उनका व्यक्तित्व भी था।अज़ीज़ उस बनारसी समाजिक ताने बाने के प्रतीक थे जिसमे काशी और काबा दोनों की साझेदारी थी।वे कबीर की परम्परा के वाहक थे।जिन बनारसी साड़ियों का दुनिया भर में जलवा है, उसे अज़ीज़ जैसे लोग ही बनाते हैं। ये अलग बात है कि दुनिया में वह पहचानी जाती है,बड़े बड़े गद्दीदारो और शोरूम वालों के ज़रिए।इन बुनकरों की हाडतोड मेहनत पर ही इनकी सम्पन्नता का तम्बू तना है।
अज़ीज़ बनारस के कॉटन मिल कम्पाउण्ड की बुनकर बस्ती में रहते थे।बनारस की कॉटन मिल बीसवीं सदी की शुरूआत में खुली और आज़ादी के बाद बंद हो गयी।पर मिल का परिसर बुनकरों की बस्ती में तब्दील हो गया।इसी बस्ती के दो कमरों के एक मकान में दो करघे लगाकर अज़ीज़ अपने नौ बच्चो और माता पिता के साथ रहते थे।घर के बाहर मैदान में वे अपनी तूरिया ( वह लकड़ी का वह गोल लठ्ठा जिसपर साड़ी का ताना लपेटा जाता है) पर तन्नी तानते। क्योंकि इस काम के लिए पन्द्रह से बीस मीटर लम्बी जगह की दरकार होती है।तूरिया पर तन्नी तानने के बाद उसे करघे पर चढ़ा बुनाई शुरू करते।पन्द्रह से बीस रोज़ में जब सामान्य साड़ी तैयार होती तो अज़ीज़ साड़ी ले जा गद्दीदार को बेचते।ख़ास साड़ी बुनने में पॉंच से छ: महीने लगते है।लेकिन गद्दी या कोठीदार उन्हे एक महीने आगे की चेक देता।अगर पैसा फ़ौरन चाहिए तो गद्दीदार के नीचे ही चेक भुनाने वाली जमात बैठी रहती जो तीन चार परसेंट काटकर चेक का नक़द भुगतान कर देते।गद्दीदार फिर बड़े बड़े होलसेलर को साड़ी देता है और वहॉं से रीटेल दुकानदारों के यहॉं साड़ी पहुँचती है।बुनकर से दुकान तक पहुँचने में साड़ी का दाम तीन से चार गुना हो जाता है।मित्रो यही है बनारसी साड़ी का अर्थशास्त्र और यही है बनारसी बुनकरो की व्यथा कथा।विसंगति देखिए बुनकर धागा नक़द ख़रीदता है और साड़ी एक महीने की उधारी पर बेचता है।
यह संयोग ही हैं। कि अज़ीज़ जहॉं साड़ी बुनते थे उसी से एक किलोमीटर दूर नरहरपुरा में कोई साढ़े चार सौ साल पहले कबीर के माता पिता नीरू और नीमा का भी करघा था।आज भी कबीर का करघा,नीरू और नीमा का कमरा कबीर की मूल गादी में सुरक्षित है।यानी सोलहवीं सदी से वह इलाक़ा जुलाहों का था।कबीर जुलाहा को जाति नहीं सृष्टि का निर्माता कहते थे।यहीं करघे पर बैठ, एक तरफ़ कबीर समाज की विसंगतियों पर चोट करते थे।दूसरी तरफ़ उनका ध्यान रहता कि धागा जहॉं कहीं टूटे, उसे ढंग से जोड़ते जाओ।ऐसा जोड़ों की धागा धागे में मिल जाए।कोई गॉंठ न पड़े।फिर टूटने की सम्भावना भी न रहे।यही कबीर के समाज का सूत्र भी है।तभी तो उन्होंने कहा
झीनी झीनी बीनी चदरिया
काहे कै ताना काहे कै भरनी
कौन तार से बीनी चदरिया
इडा पिङ्गला ताना भरनी
सुखमन तार से बीनी चदरिया
आठ कँवल दल चरखा डोलै
पाँच तत्त्व गुन तीनी चदरिया
साँ को सियत मास दस लागे
ठोंक ठोंक कै बीनी चदरिया
सो चादर सुर नर मुनि ओढी,
ओढि कै मैली कीनी चदरिया
दास कबीर जतन करि ओढी,
ज्यों कीं त्यों धर दीनी चदरिया
इससे लगता है कबीर के लिए करघा ही जीवन था। क्योंकि वह कर्म भी है। ज्ञान भी है और भक्ति भी है ।कबीर से ही बनारस में कपड़ा बुनने का व्यवस्थित सिलसिला मिलता है।लेकिन कबीर से पहले भी वैदिक काल में बनारसी कपड़ों का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि बुद्ध के अंतिम संस्कार के लिए बनारस से मलमल मंगाया गया था। बौद्ध साहित्य के मुताबिक़ बुद्ध ने मरने से पहले आनंद से कहा ” मेरे मरने पर मेरी अंत्येष्टि चक्रवर्ती सम्राट की तरह करना। वह कैसे? पूछने पर बुद्ध ने बताया। शव को नहला कर नवीन वस्त्र में लपेटना, फिर नये रूई से ढकने के बाद शव को पुनः नवीन कपड़े में लपेट कर लोहे की द्रोणी में रखना। शव को द्रोणी सहित चिता पर रखना। (आप जानते होंगे बुद्ध की इसी द्रोणी में बची अस्थियों को उस समय वहां मौजूद सात राजाओं ने अपने अपने राज्यों में ले जाकर स्तूप बनवाये थे।)
अब इस घटना से इतना तो तय ही हो जाता है कि काशी की वस्त्र परंपरा बुद्ध से भी पुरानी है। अज़ीज़ भाई के बहाने इस वस्त्र परंपरा के इतिहास में भी भ्रमण हो गया। बनारसी कपड़ों में सोने ( जरी ) का इस्तेमाल कब हुआ यह स्पष्ट नहीं है। वेदों में हिरण्यमयी वस्त्र आता है।स्वर्ण की उपस्थिति को शुद्धता का प्रतीक माना गया। उस दौर में कपड़ो पर जरी या सोने का कहीं उल्लेख नही मिलता।यहां तक कि प्राचीन मंदिरों में आभूषण तो दिखते हैं।पर सुनहले वस्त्र नहीं दिखाई देते।अजंता की गुफाओं की पेन्टिंग में भी नहीं। जरी या जरदोजी के लिए सोने के बारीक तार की कला मुगलों के साथ भारत आयी।जहांगीर ने ईरान से एक तारकश बुलवाया ऐसा उल्लेख मिलता है।तो यहीं से होती है भारत में जरी की शुरूआत।
जरी मुगल काल में फली-फूली, जब किमखाब से बने वस्त्रों का चलन था, जिसे राजा-महाराजा खास मौके पर पहनते थे। ‘हिरण्य द्रापि’ नामक वस्त्र संभवतः किमखाब की कसीदाकारी से बनता था। अथर्ववेद के मुताबिक नवविवाहिता वधू जिस पालकी में बैठती थी, उसमें सुनहरी कलाबत्तू की चादर बिछाई जाती। इस पर जरी का काम है, जिसे जरदोजी भी कहते है। इस फारसी शब्द का अर्थ है—सोने की कढ़ाई। कलाबत्तू रेशम के धागे पर लपेटा सोने-चाँदी का तार होता है, जिससे कपड़े पर बेल-बूटे बनते हैं। गुप्तकाल में सोने के घोल में सूत को रँगकर कलाबत्तू बनता था।
अज़ीज़ मियां बनारस की इस प्राचीन और युगीन परंपरा के आधुनिक नायक थे। वह सिल्क जरदोजी के उस्ताद थे।मेरे घर अक्सर आते।मेरे यहॉं साड़ियाँ उन्हीं से ली जाती।दोस्त मित्र और बृहत्तर परिवार के लोगों को भी मैं अज़ीज़ से ही साड़ी दिलवाता।वजह उनसे सीधे लेने साड़ी काफ़ी सस्ते में मिलती।और बीच से कोठीदार, थोक और रीटेल व्यापारी का मुनाफा ग़ायब होता ।हमें साड़ियाँ सस्ती मिलती और अज़ीज़ को पैसा भी तुरंत मिलता।इसलिए अज़ीज़ से अपना घरोपा बढ़ता रहा।अज़ीज़ बनारसी साड़ी की कोई डिज़ाइन देने पर उसी तरह का बुन भी देते थे।आदमी शालीन थे।किसी से अपनी लाचारी नहीं बताते थे।हंसी मज़ाक़ में उनका मन रमता था।
अज़ीज़ साड़ी बुनते और बेचते,इस मज़दूरी से होने वाली आमदनी से ही उनका परिवार पलता था।परिवार बड़ा था और आय के कोई और स्त्रोत नहीं थे।मेहनत और भोजन के इस अर्थशास्त्र में उनके जीवन का इकलौता मक़सद ‘हज’ पूरा नहीं हो पा रहा था।अज़ीज़ हर साल हज पर जाने के लिए पैसे जोड़ने की कोशिश करते मगर तब तक उनके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंज जाती। फिर क्या था, नवजात की सेवासुश्रुषा में पैसे खर्च हो जाते और अज़ीज़ का हज टल जाता। हज का इन्तज़ार करते करते उनके नौ बच्चे हो गए।हर साल होने वाले बच्चे से उनका बजट तो बिगडता पर फ़ायदा यह होता कि बड़े होने पर यही बच्चे उनके साथ खड्डी और करघे पर बैठने लगते और उन्हें हेल्पिंग हैण्ड मिल जाते।
धीरे धीरे अज़ीज़ मेरे घरेलू हो गए। मैं जब भी छुट्टियों में बनारस जाता अज़ीज़ मिलने ज़रूर आते।एकबार अज़ीज़ ने मुझसे कहा कि हर मुसलमान की एक ही इच्छा होती है हज पर जाने की। मेरी भी है।कोशिश कई साल से कर रहा हूँ पर जा नही पा रहा हूँ। आप चाहें तो सरकार के कोटे से मुझे भिजवा सकते है। मैंने पूछा यह कौन सा कोटा है? वे बोले हाजियों की संख्या के आधार पर सरकार अपने खर्चे से ख़ादिम भेजती है।वे हाजियों की सेवा देखभाल के लिए जाते है। इन्हे ‘ख़ादिम-उल-हुज्जाज’ कहा जाता है। हज कमेटी के खर्च पर सउदी जाने वाले यह खादिम हज के दौरान हाजियों की मदद करते हैं और देश में उनके परिवार वालों से संपर्क में रहते हैं।
यह भी पढ़ें : हीरु पानवाले : हेमंत शर्मा की इतवारी कथा
तब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। उसके हजमंत्री एजाज़ रिज़वी थे।एजाज़ रिज़वी कोई बड़े नेता नहीं थे।सरकार में सिर्फ़ अल्पसंख्यक प्रतिनिधि के नाते मंत्री बने थे। मैने अज़ीज़ भाई से दरखास्त लिखवाई और मंत्री जी से निवेदन किया कि ये मेरे जानने वाले हैं।मैंने इनसे वायदा किया है कि तुम्हें हज पर भेजूँगा।आप इसे अपनी सरकारी सूची में शामिल कर ले।ख़ादिम कोटे में जाने की कई शर्तें थी। एक -पहले कभी आप उमरा के लिए गए हो।दो- आपको अरबी आती हो,आदि आदि।इंटरव्यू में अज़ीज़ भाई से पूछा कि आप अरबी जानते हैं।अज़ीज़ ने कहा “जेतना बोलित है ओतना जानित है। न पढे जानित है न लिखे।“ एजाज रिज़वी भले आदमी थे। कहा ‘पंडित जी ये कुछ जानते नहीं हैं। पर आपका हज का वायदा हम ज़रूर पूरा करेंगे।’
अज़ीज़ का नाम सरकार द्वारा भेजे जाने वालो की सूची में आ गया। मुझे इस कदर ख़ुशी हुई कि लगा मैं ही हज पर जा रहा हूँ।लेकिन अज़ीज़ के घर में मामला फँस गया। उनके पिता जीवित थे और उनकी परम्परा में पिता को हज कराए बिना बेटा हज पर नहीं जा सकता। सो अज़ीज़ का मामला लटक गया। मैंने कहा कोई बात नही। फिर मशक़्क़त की। सूची में नाम बदलवा उनके वालिद का नाम जोड़ा गया और अज़ीज़ के वालिद हज की मुकद्दस यात्रा पर चले गए। मैंने अज़ीज़ से अगले साल उन्हें भी भिजवाने का फिर वायदा किया।अज़ीज़ मियाँ के लिए यह डबल धमाका था। दूसरे साल मैंने ठौर बदला। इस बार अज़ीज़ की दरखास्त मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेन्द्र मिश्र के यहॉं लगाई। नृपेन्द्र जी ने अज़ीज़ का नाम ख़ादिमों की सूची में डलवा उन्हें भी हज पर रवाना करवा दिया। हज से लौट कर अज़ीज़ अब हाजी अज़ीज़ हो गए। काशी से काबा का सफ़र पूरा कर आए। लौट कर अज़ीज़ ने अपने यहॉं दावत रखी।मुझे फ़ोन किया आपका आना ज़रूरी है। मैंने कहा, अज़ीज़ भाई काशी में रहते हो और काबा हो आए अब बचा का यार ? मौज करो।
यह भी पढ़ें : चूँ चूँ करती आई चिड़िया-हेमंत शर्मा
एक तो अज़ीज़ मियाँ का स्नेह और दूसरे बनारस हमारी कमजोरी।मैं हमेशा बनारस जाने का बहाना ढूँढा करता हूँ।सो, मैं गया। बुनकर बस्ती में मेरा बड़ा जलवा हुआ। अज़ीज़ के रिश्तेदार मेरा हाथ चूम रहे थे।अज़ीज़ मियां के चेहरे पर एक अद्भुत संतोष दिखाई दे रहा था।मानो वे अब जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हों।कोई और ख्वाहिश बाकी न रह गई हो। इसी संतोष भरे जीवन के साथ एक रोज़ अज़ीज़ ने आंखे मूंद लीं। उनके बाद उनके बेटे शम्सुल ने काम सम्भाला।लेकिन अब वो बात नहीं थी।न बुनकारी में, और न ही व्यवहार में। उनका बेटा सिर्फ़ चरक और छोटे छोटे काम करने लगा। अज़ीज़ भाई का हुनर और उनकी शख्सियत दोनो ही, उनके साथ विदा हो गई। उत्तराधिकार में रह गईं तो उनकी यादें। जब कभी भी बनारसी साड़ी का जिक्र होता है, अज़ीज़ भाई की याद ज़ेहन के किसी कोने में दस्तक देने लगती है।मुझे हमेशा से लगता आया है कि बनारस को समझने के लिए आपको कबीर को पढ़ना पढ़ेगा और किसी अज़ीज़ से मिलना पड़ेगा।मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ये दोनो ही नेमतें हासिल हुई।
[better-ads type=”banner” banner=”100781″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]